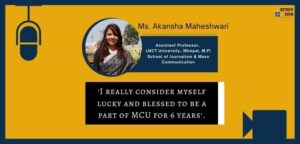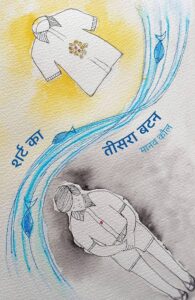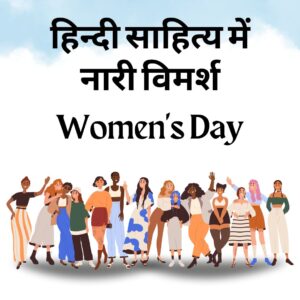शिक्षा से संसार चमकता है, युग-युग आगे बढ़ता है ।
अंध-कूप से निकला मानव, कदम चांद पर रखता है।
हमारे जीवन में किसी भी परिवार में बच्चे के जन्म लेते ही बच्चा जैसे – जैसे बड़ा होता है ठीक वैसे-वैसे मां द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह मातृभाषा के रूप में सर्वप्रथम सीखता है और फिर घर के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करना सीखता है ।
आजकल तो बच्चा तीन साल का हुआ कि पाठशाला में पढ़ने-लिखने के लिए भेजा जाता है । फिर बच्चा अपने माता-पिता और पाठशाला में पढ़ने-लिखने के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है । जिस वातावरण में पालन-पोषण होता है, उसका और आस-पड़ोस के माहोल, भाषा इत्यादि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वही सीखने की कोशिश करता है ।
प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली के तहत सुशिक्षित बनाने हेतु प्रयासरत रहते हैं । इसीलिए भाषा का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है या हम यह कह सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । बच्चे भाषा के माध्यम से ही हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं । हमारे भारत देश में ही आप देखिएगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाषा में परिवर्तन आ जाता है और यही भाषा ही हमें एक-दूसरे के साथ से कार्य करने हेतु सहयोग करती है ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, और भारत में कई भाषाएं बोली जाती है पर यहां पर एक भी भारतीय भाषा नहीं है जो पूरे देश में बहुमत से बोली जाती है| जैसे कि हिंदी भाषा उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है परंतु इसका उपयोग दक्षिण भारत में काफी कम है, इसी तरह दक्षिण भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, मलयालम और तेलुगु का प्रयोग उत्तर भारत में बहुत ही कम होता है|
भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर अनेक भाषाएं ऐसी बोली जाती है जिनमें बहुत ही कम अंतर है और इस अंतर के कारण उन्हें एक भाषा माना जाए या दो या तीन, यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है| 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 122 भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के आठवें कार्यक्रम में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध हैं|
1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,652 “मातृभाषा” या भाषा का इस्तेमाल किया जाता था| लेकिन 1971 की जनगणना के अनुसार केवल 108 भाषाओं को भारत की भाषाओं में शामिल किया गया और उन भाषाओं को हटा दिया गया जिनको बोलने वालों की संख्या 10 हजार लोगों से कम थी । सन 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार यह पाया गया कि भारत में 122 भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 हजार लोगों से अधिक है अतः इस आंकड़े के अनुसार यह माना जाता है कि-
- भारत में लगभग 122 भाषाएं बोली जाती है|
- भारत में 29 भाषाएं ऐसी हैं उनको बोलने वालों की संख्या 1000000 (दस लाख) से ज्यादा है|
- भारत में 7 भाषाएं एसी बोली जाती है जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है|
- भारत में 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10000 (दस हज़ार) से ज्यादा है ।
मेरा उपर्युक्त भाषा का विश्लेषण बताने का उद्देश्य यही है केवल की भाषा की भूमिका इतनी विशाल है कि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने किसी भी स्थान पर जाएं तो वहां की भाषा अवश्य रूप से ही सीखने की कोशिश करें क्यो कि बचपन से ही सीखेंगे तभी तो वे अपना विकास अधिक सूदृढ करने में कामयाब होंगे ।
आजकल हम देख रहे हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों को जरूरत पड़ने पर अपनी संबंधित शिक्षा ग्रहण करने, नौकरी या व्यवसाय करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, तब बचपन से लेकर आजीविका चलाने तक आपने जो भी शिक्षा या ज्ञान भाषा के माध्यम से प्राप्त किया है, उसी का प्रभाव मिलने-जुलने वाले लोगों पर पड़ता है और जिसका प्रतिफल काम पूर्ण होने के रूप में प्राप्त होकर सफल होता है ।
मैं अपने बच्चों को हमेशा ही कहती हूं कि अपनी पुस्तकों का अध्ययन तो करना ही है पर साथ ही साथ समाचार पत्र तो अवश्य रूप से ही पढ़ना चाहिए । आप जो भी भाषा का अध्ययन करते हैं या ज्ञान रखते हैं, तो उसी भाषा में टीवी पर प्रसारित समाचारों को भी अवश्य देखिए, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं तो उतना ही आपका आत्म विकास प्रबल होता है । मेरा तो मानना है कि जहां से भी ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ग्रहण करते रहना चाहिए, क्यो कि शिक्षा का कभी भी अंत नहीं होता है ।
वस्तुतः शिक्षा हमारे अन्तःकरण को , चरित्र को शुचिता प्रदान करती है । हमारी प्रतिभाओं को विकसित करने का संबल बनाती है, हममें पूर्ण रूप से विकास लाती है, हमारी सुंदरतम विभूतियों को इस प्रकार संवारती है कि उसमें न केवल हमारा ही अपितु समाज का भी कल्याण हो अर्थात व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय स्थापन का कार्य भी शिक्षा के सौजन्य से होता है ।
“विद्यालय की कक्षाओं में भारत देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है ।” अतएव विद्यार्थियों को ऐसी अमूल्य शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे अनुशासन एवं शालीन आचरण के साथ-साथ धैर्य, ईमानदारी, सहनशीलता, सद्भावना, निष्पक्षता, कर्त्तव्य परायणता प्रभुति गुणों को आत्मसात कर सकें और इन अर्जित गुणों को लेकर भविष्य में वे समाज में समीचीन ढंग से सम्पृक्त हो सकें ।
इन सभी गतिविधियों में शिक्षक जो है सर्वप्रथम भूमिका निभाते हैं , अतः वे अपनी पाठशाला या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की रूचि के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जैसे अभिनय, संगीत, नृत्य आदि हदयस्थ भावनाओं को जागृत एवं उजागर करने के मुख्य साधन होते हैं । इसके अलावा बौद्धिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन के प्रति जागरूक होते हुए वाद-विवाद, परिसंवाद, गोष्ठी, तात्कालिक- भाषण, अन्त्याक्षरी, कविता, कहानी, निबंध- लेखन प्रभृति प्रतियोगिताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए । ऐसा करने से विद्यार्थियों में वैचारिक एवं सृजनात्मक क्षमता का वर्धन होगा, जिसके संस्पर्श से शिक्षा सफल व्यक्ति पूर्णकाय हो जाती है । एन.सी.सी., स्काउटिंग, राष्ट्रीय-सेवा योजना आदि के द्वारा भी विद्यार्थियों में ऐसी भावनाओं को जागृत एवं उदीप्त किया जा सकता है, जिसके सहारे वह समाज और राष्ट्र से जुडकर लोक मांगलिक कार्य का सम्पादन कर सकते हैं । इससे उनके चरित्र में सौष्ठव लक्षित होगा तथा लोकोपकारक की मंजुल छवि उसके व्यक्तित्व में थिरकने लगेगी ।
उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन का निष्कर्ष यही है कि शिक्षा का जो उदात्त उद्देश्य है, वह पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है । शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का शिक्षण ही यथेष्ट नहीं है, साथ ही साथ सहगामी गतिविधियों के आयोजन की भी नितांत आवश्यकता है और इन सभी में भाषा का अपना अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग महत्व है , जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती है । ऐसी शिक्षा समस्त विद्यार्थियों को हर स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी तो देश का भविष्य और हर विद्यार्थी का भावी जीवन अवश्य ही उज्जवल होगा ।
अंत में आप समस्त पाठकों को आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करती हूं कि आप सभी मेरा यह लेख पढ़िएगा एवं अपने विचार व्यक्त किजिएगा ।
~ आरती अयाचित
स्वरचित एवं मौलिक
भोपाल